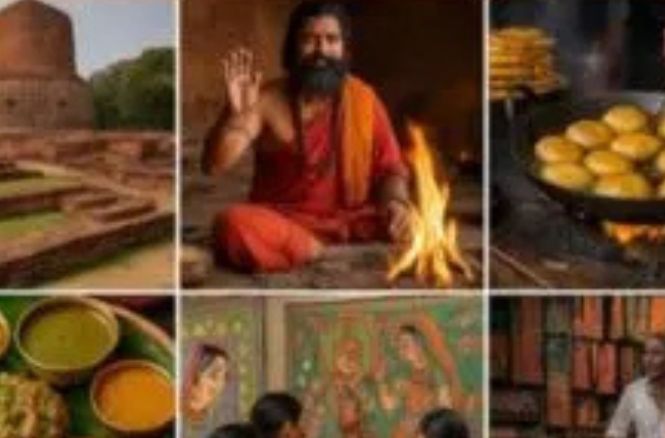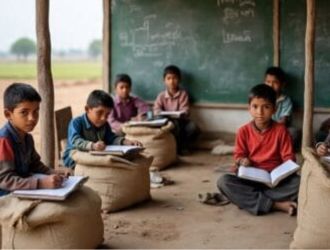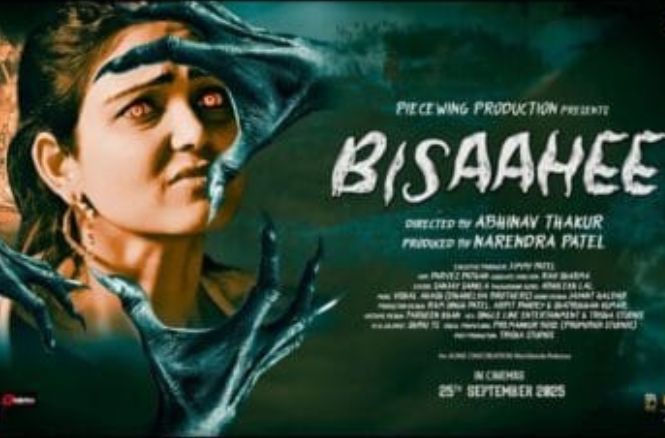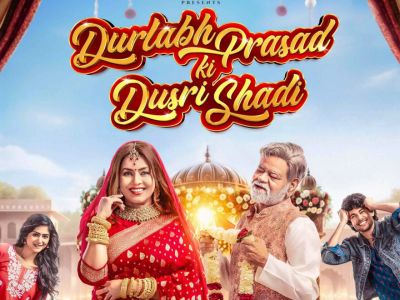AI Image
चीनी मिलें: जहाँ मीठी ख़ुशबू अब सिर्फ़ यादों में है
एक ज़माना था जब बिहार की सुबह की पहचान गन्ने की मीठी ख़ुशबू और चीनी मिलों की भाग-दौड़ से होती थी। साल 1980 के दशक में, हमारे पास 28 चीनी मिलें थीं, और यह आकंड़ा देखिए—हम देश के कुल चीनी उत्पादन में 30% का बड़ा हिस्सा थे। मोतिपुर, बेतिया, लौरिया—ये शहर महज़ नक़्शे पर बिंदु नहीं थे; ये रोज़गार और उम्मीद के केंद्र थे। मोतिपुर शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, वह अपनी बुलंदी के दिनों में रोज़ाना 1,200 टन गन्ना पीसती थी और 1,200 क्विंटल चीनी तैयार करती थी। मगर धीरे-धीरे, 90 के दशक में, कहानी बदलने लगी। पुरानी मशीनें, गन्ने की बढ़ती लागत, और सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार और राजनीतिक अनदेखी की थी। 1996-97 में जब मोतिपुर मिल बंद हुई, तो यह सिर्फ़ एक फैक्ट्री का शटर डाउन नहीं हुआ; 25,000 मज़दूरों की ज़िंदगियाँ अंधेरे में चली गईं। आज, हमारे पास मुश्किल से 9 मिलें चल रही हैं, और देश के चीनी उत्पादन में हमारा योगदान सिमटकर मात्र 2% रह गया है। यह आँकड़ा नहीं, यह लाखों लोगों की ख़ामोशी है।
भागलपुर की सिल्क: धागों का जादू कहाँ खो गया?
भागलपुर को कभी दुनिया “सिल्क सिटी” के नाम से जानती थी। यहाँ के बुनकरों के हाथों में एक अजीब जादू था, जो रेशम के धागों को सजीव बना देता था। 1972 में “बिहार स्पन सिल्क मिल” की शुरुआत हुई थी, एक नई सुबह की उम्मीद लेकर। मगर अफ़सोस, वह सुबह भी ज़्यादा देर टिक न पाई और 1993 में मिल बंद हो गई। नाथनगर के 6,000 बुनकर परिवार अचानक ख़ुद को बेसहारा महसूस करने लगे। रही-सही कसर चीन की सस्ती सिल्क ने पूरी कर दी, जिसने बाज़ार को इस तरह पटका कि हमारे बुनकरों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 2020 तक, लगभग 95% उद्योग ढह चुके हैं, और करघे की खटखटाहट की जगह अब सिर्फ़ एक उदास सन्नाटा है।
खंडहरों की ख़ामोशी: बकाया वेतन और अधूरे सपने
मोतिपुर के खंडहरों की टूटी दीवारों पर आज भी मजदूरों के नाम लिखे हैं—ताहिर, फ़ाइज़ुल, सियाराम सिंह। ये नाम नहीं हैं, ये दर्द की आवाज़ें हैं। बाईस साल बीत गए, लेकिन इन मज़दूरों को आज भी उनका बकाया वेतन नहीं मिला है। कल्पना कीजिए उस पिता की, जिसकी बेटी की शादी बकाया पैसों के इंतज़ार में अटकी होगी, या उस बेटे की, जो रोज़गार की तलाश में अपना गाँव छोड़कर दिल्ली की अज्ञात भीड़ में गुम हो गया होगा। ये खंडहर सिर्फ़ ईंट-पत्थर के अवशेष नहीं हैं; ये उन टूटे हुए सपनों और बिखरी हुई ज़िंदगियों के गवाह हैं, जिन्हें व्यवस्था ने समय पर इंसाफ़ नहीं दिया।
वादे और हक़ीक़त: अंतहीन चक्र का दर्द
हर चुनाव आता है, और वही मीठा जुमला दोहराया जाता है—”बंद मिलें फिर से शुरू होंगी।” मज़दूरों के लिए, ये अब वादे नहीं रहे; ये एक पुराना, थका देने वाला गीत बन चुके हैं, जिसे बार-बार सुना जाता है, लेकिन इसकी धुन कभी पूरी नहीं होती। बड़े-बड़े नेताओं के बड़े-बड़े बयान, जैसे कि “सभी बंद चीनी मिलें फिर से शुरू की जाएंगी,” अब एक दूर की ख़बर जैसे लगते हैं—सुना तो जाता है, पर यक़ीन नहीं होता। तीन दशक बीत चुके हैं, और इस अंतहीन इंतज़ार से थके हुए लोग अब भी एक सवाल पूछते हैं, जिसमें आशा कम और हताशा ज़्यादा है: “क्या हमारी मिलें फिर से चलेंगी?”
फिर से चिंगारी जलाने की ज़रूरत
अगर बिहार को वाकई अपने पुराने गौरव की तरफ़ लौटना है, तो अब केवल जुबानी जमा-खर्च से काम नहीं चलेगा। हमें ईमानदार कार्रवाई करनी होगी—मिलों का आधुनिकीकरण करना होगा, प्रबंधन में पारदर्शिता लानी होगी, और सबसे अहम, बुनकरों और किसानों को सीधा सहारा देना होगा। बिहार की मिट्टी में आज भी मेहनत की ताक़त बाकी है। हमें बस एक ऐसी ईमानदार चिंगारी की ज़रूरत है जो इन ख़ामोश खंडहरों में एक बार फिर से जीवन की गर्माहट और रोज़गार की रौशनी भर सके।