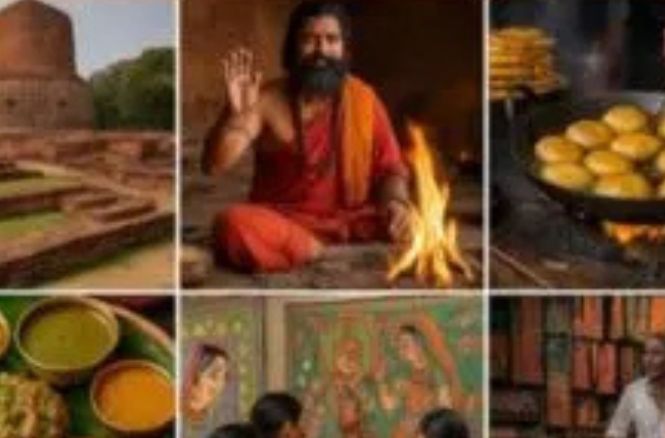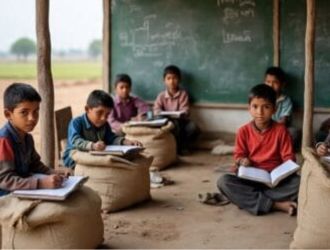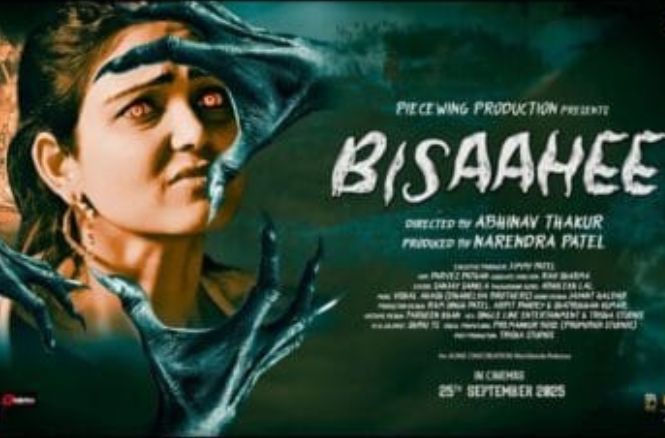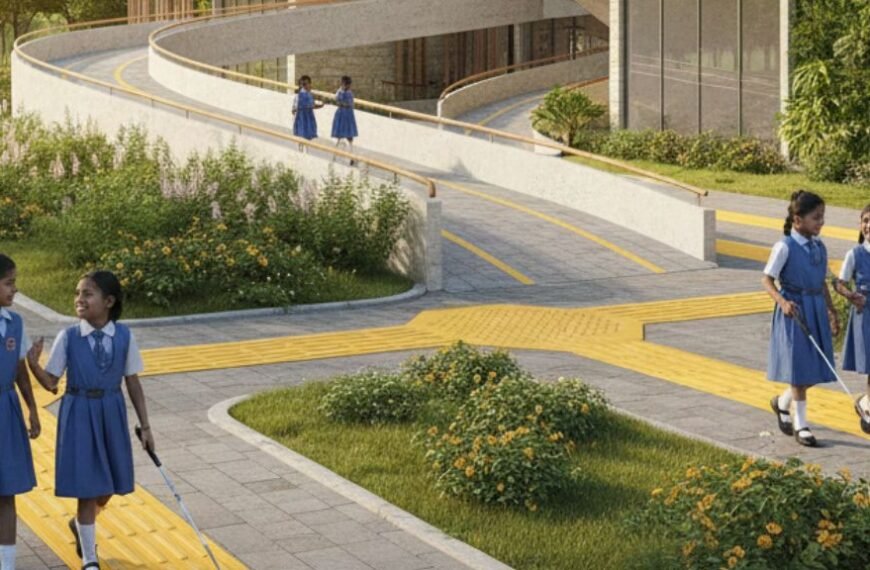बिहार के मधुबनी जिले में एक छोटा सा गाँव है—सौराठ। यह गाँव अपनी सौराठ सभा के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यह कोई आम बाज़ार नहीं, बल्कि मैथिल ब्राह्मण परिवारों के लिए सदियों पुरानी एक अनोखी ‘वैवाहिक मंडी’ थी। 700 साल पहले शुरू हुई यह परंपरा, सिर्फ शादी कराने का मंच नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करती थी कि रिश्ता सही कुल और परंपरा के हिसाब से हो ।

जब राजा ने रखी थी नियम की नींव
इस सभा की शुरुआत से पहले भी रिश्ते तय होते थे, लेकिन वंशावली का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था। इस परंपरा की नींव 14वीं सदी में कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव ने रखी थी (1326 ई.) । राजा ने देखा कि समाज में कई तरह की परेशानियाँ थीं, खासकर ऊँचे कुल के कुछ पुरुष कई शादियाँ करते थे, जिससे युवा विधवाओं की संख्या बढ़ रही थी ।
इन सामाजिक मुश्किलों को रोकने और खून की पवित्रता (शुद्धता) बनाए रखने के लिए पंजी प्रबंध नाम का एक कठोर नियम बनाया गया । इस नियम के तहत पंजीकार (Panjikar) नाम के आधिकारिक रिकॉर्ड रखने वाले नियुक्त किए गए ।
पंजीकार का काम: इन पंजीकारों के पास परिवारों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी का हिसाब (वंशावली) हाथ से लिखे रिकॉर्ड (पंजी) में रहता था । सभा में जब कोई संभावित रिश्ता बनता, तो पंजीकार दोनों परिवारों के गोत्र (कुल) और मूल (पैतृक गाँव) की जाँच करते थे । नियम साफ़ था: पिता के पक्ष से सात पीढ़ी और माँ के पक्ष से पाँच पीढ़ी तक कोई खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए । अगर सब सही पाया जाता, तो पंजीकार सिद्धांत पत्र नाम का एक प्रमाण पत्र जारी करते थे, जो शादी के लिए ज़रूरी ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ जैसा था । इस पत्र के बिना मैथिल समाज में शादी को सही नहीं माना जाता था ।
सभा गछी: उम्मीदों का बाग
यह ऐतिहासिक सभा मधुबनी से लगभग 6 किलोमीटर दूर, 22 एकड़ में फैले आम, पीपल और बरगद के पेड़ों वाले सभा गछी में आयोजित होती थी । ज्येष्ठ-आषाढ़ (जून-जुलाई) के महीने में, शुभ विवाह के दिनों (शुद्ध) पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे ।
यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अनोखा होता था। दूर-दराज़ से आए दूल्हे और उनके पिता खुले मैदान में डेरा डालते थे, जहाँ वे एक तरह से ‘सार्वजनिक प्रदर्शन’ पर होते थे । दुल्हन के पिता अपने रिश्तेदारों और घटक (बिचौलिये) की मदद से, लड़के की योग्यता (इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी) और परिवार के कुल को देखते हुए रिश्ते की तलाश शुरू करते थे। यह एक ऐसा मंच था जहाँ हर सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बिना ज़्यादा भटकन के योग्य रिश्ता तलाश लेते थे ।
विडंबना और पतन के दर्दनाक कारण
इस परंपरा का एक दुखद पहलू भी था: सभा स्थल पर महिलाओं को आने की इजाज़त नहीं थी । यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ महिलाएँ अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले में सीधे शामिल नहीं हो सकती थीं, जबकि मिथिला का इतिहास सीता के स्वयंवर की उदार परंपरा से जुड़ा है ।
आज यह 700 साल पुरानी विरासत ख़त्म होने की कगार पर है। जहाँ पहले लाखों लोग आते थे , अब मुश्किल से 50-100 लोग ही आते हैं । इस पतन के पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है:
- दहेज का बाज़ार: इस सभा ने धीरे-धीरे योग्य दूल्हों का एक खुला ‘बाज़ार’ बना दिया , जहाँ दूल्हे की योग्यता के अनुसार दहेज की खुली बोलियाँ लगती थीं । माता-पिता अपने बेटे की शिक्षा में किए गए ‘निवेश’ पर वापसी के रूप में दहेज को देखने लगे ।
- वर-अपहरण (पकड़ुआ शादी): 1980 और 90 के दशक में, जब दहेज की मांगें असहनीय हो गईं, तो कुछ लड़कियों के परिवारों ने पकड़ुआ शादी (वर-अपहरण) का रास्ता अपनाया । योग्य इंजीनियर्स और डॉक्टरों को जबरन उठाकर, बंदूक की नोक पर शादी कराई जाने लगी । इस खौफ के कारण, ऊँचे पेशेवर वर्ग के लड़कों ने सभा में आना बंद कर दिया, जिससे इस संस्था की प्रतिष्ठा गिर गई ।
- आधुनिकीकरण और बदनामी: मीडिया ने इसे ‘दूल्हा बाज़ार’ कहकर बदनाम किया, जिससे आधुनिक परिवार इससे दूर हो गए । साथ ही, नौकरी की तलाश में शहरों में पलायन और ऑनलाइन वैवाहिक साइटों के उदय ने पंजीकार और घटक पर निर्भरता को खत्म कर दिया है ।
आज, सरकार इस इतिहास को बचाने के लिए पंजी पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का प्रयास कर रही है । लेकिन पंजीकार डरते हैं कि उनका सदियों पुराना, गोपनीय ज्ञान अगर सबके लिए खुल गया, तो उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी । सौराठ सभा का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि क्या मिथिला समाज अपनी परंपरा की पवित्रता को दहेज और रूढ़िवादिता के अभिशापों से मुक्त करके आधुनिकता के साथ जोड़ पाता है।