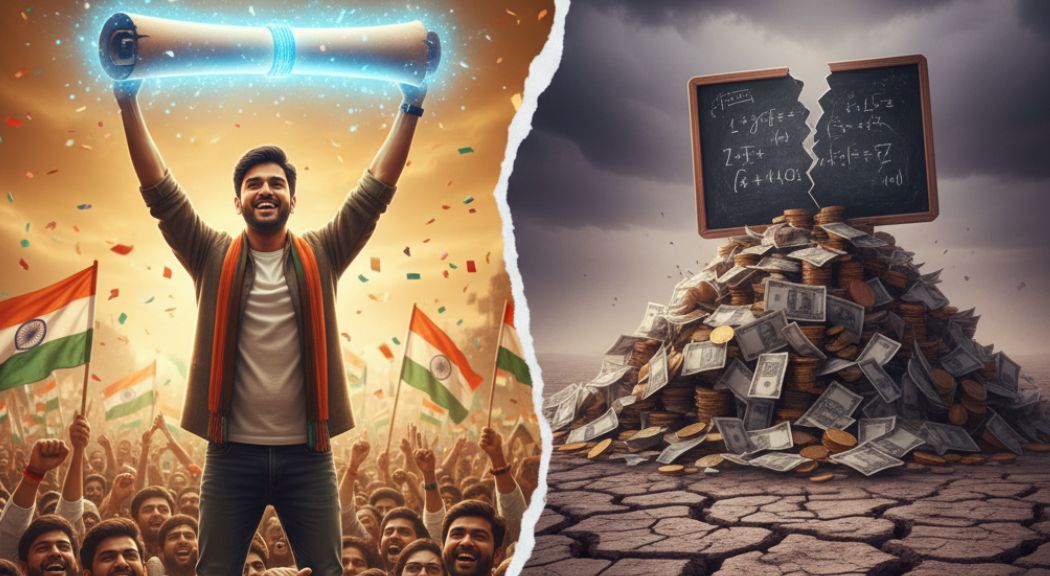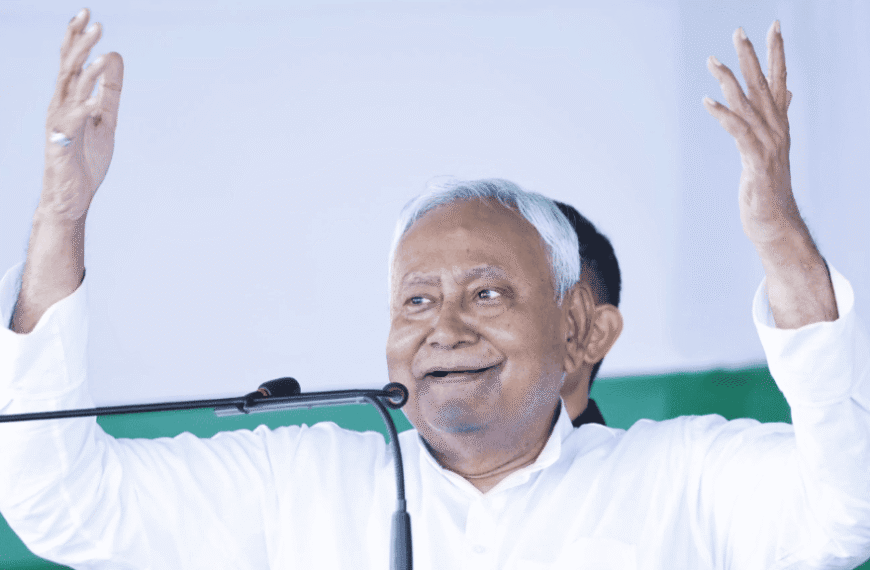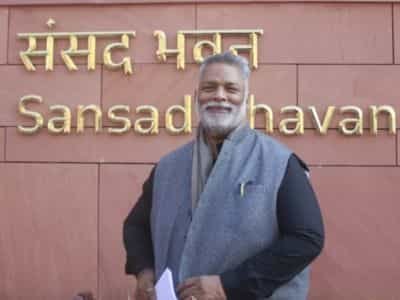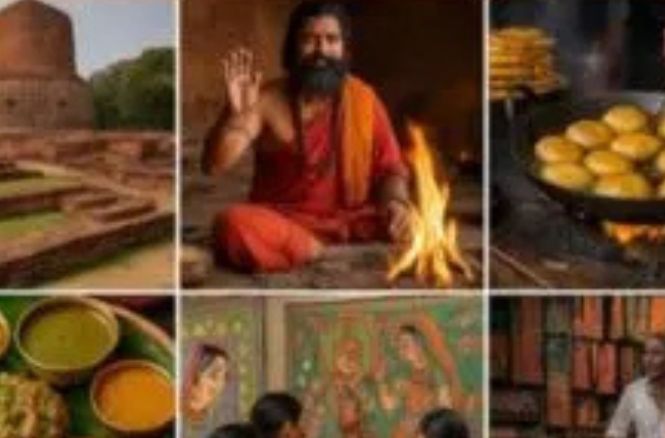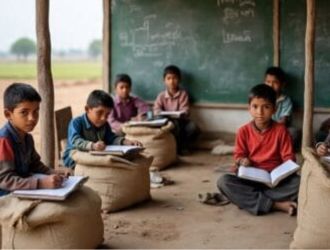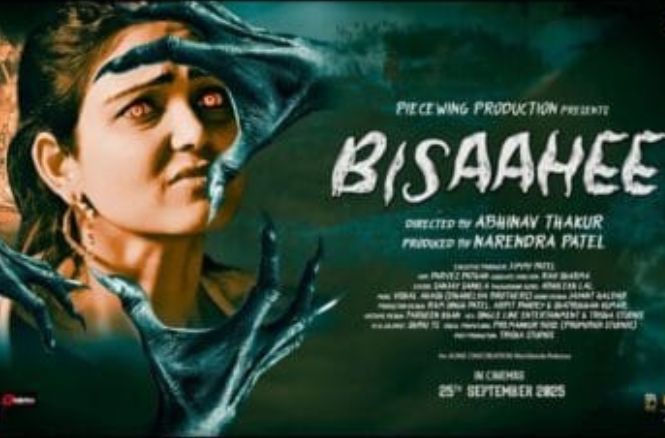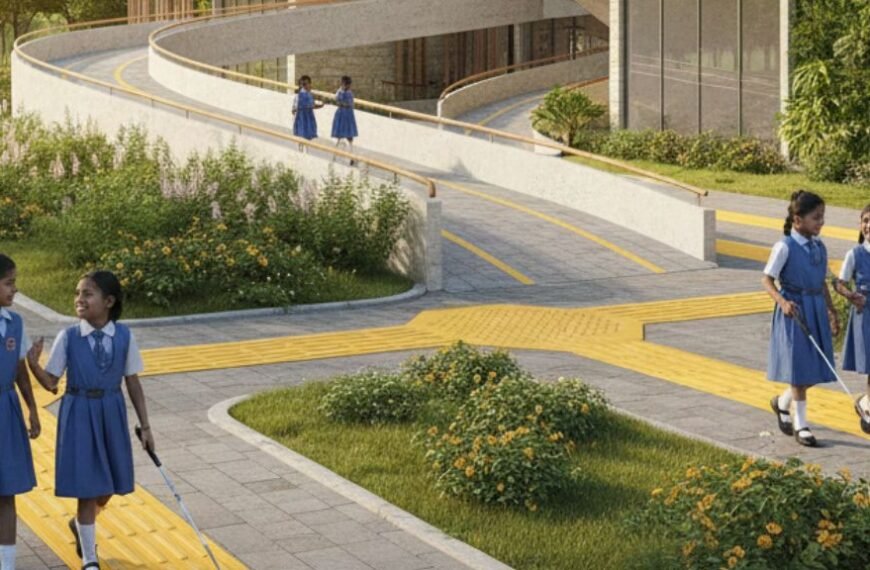राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर ‘हर परिवार को सरकारी नौकरी’ देने का जो वादा किया, वह युवाओं के लिए एक सपना जैसा था। मोटे तौर पर, इस वादे का मतलब है लगभग 2.5 करोड़ नई सरकारी नौकरियाँ पैदा करना। यह आंकड़ा सुनने में जितना शानदार लगता है, हकीकत की कसौटी पर यह उतना ही असंभव है।यह वादा उस प्रेमी की तरह है जो अपनी प्रेमिका से ‘चाँद-तारे तोड़ लाने’ की बात करता है। वादा सुनकर मज़ा आता है, लोग खुश होते हैं, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इसे सच मानकर जीवन का बड़ा फैसला नहीं लेता।

AI Image
इस विश्लेषण का मकसद यही है कि हम इस मीठे वादे को कठोर आर्थिक आँकड़ों के सामने रखकर साबित करें कि यह सिर्फ एक अव्यावहारिक (impractical) चुनावी नारा नहीं है, बल्कि यह बिहार की पहले से ही कमजोर आर्थिक सेहत के लिए विनाशकारी है।
यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों पर जोर देना RJD की मूल समाजवादी विचारधारा के भी विपरीत है। पार्टी का जन्म समाज के सबसे गरीब, भूमिहीन और पिछड़े वर्गों के लिए काम करने के लिए हुआ था। इतनी बड़ी उच्च-वेतनभोगी क्लास (High-Salaried Class) बनाने से समाज के सबसे निचले तबके को शायद ही कोई सीधा लाभ मिलेगा। यह नीति निजी व्यापार और सबसे महत्वपूर्ण, कृषि क्षेत्र को नज़रअंदाज़ करती है। एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था तब बनती है जब गाँवों और निजी क्षेत्रों में काम बढ़ता है, न कि जब पूरा राज्य सिर्फ सरकारी सैलरी पर निर्भर हो जाए।
हिसाब: सपने या सिर्फ़ बातें?
बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है (Registrar General, India, 2023 अनुमान)। औसतन 5 लोगों प्रति परिवार मानें तो राज्य में लगभग 2.6 करोड़ परिवार हैं।
इसका अर्थ हुआ कि राज्य को लगभग करोड़ों नई सरकारी नौकरियाँ बनानी होंगी — यानी राज्य की कामकाजी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी वेतनभोगी बन जाएगा।
व्यवस्था का पतन
इतनी भारी संख्या में सरकारी भर्ती का मतलब है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य-नियंत्रित (State-Driven) हो जाएगी। निजी व्यापार, स्टार्ट-अप्स, और खेती-किसानी जैसे उत्पादक इंजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ये इंजन ही राज्य की कुल कमाई (GSDP) का आधार हैं।
यह मॉडल एक ‘आत्मघाती आर्थिक चक्र’ पैदा करता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कहाँ से आती है? यह नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स से आती है। अगर राज्य के ज़्यादातर काम करने वाले लोग खुद सरकारी कर्मचारी बन जाएँगे, तो टैक्स देने वाले निजी क्षेत्र का आधार तेज़ी से सिकुड़ जाएगा। नतीजा यह होगा कि राज्य की कमाई स्थिर हो जाएगी या घट जाएगी, जबकि खर्च आसमान छूने लगेगा। करोड़ों लोगों को सरकारी पगार पर रखने का मतलब है कि एक विशाल ‘गैर-उत्पादक’ वर्ग बनाना, जो राज्य को वित्तीय अस्थिरता और संरचनात्मक विनाश की ओर ले जाएगा।
कर्ज का पहाड़ और खर्च की सीमा
बिहार पहले से ही कर्ज के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। 2025-26 के अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार पर कुल कर्ज राज्य की कुल कमाई (GSDP) का 37.04% होगा, जो करीब ₹4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यह कर्ज भविष्य में विकास के लिए उपलब्ध पूंजी को कम करता है और ब्याज भरने में ही राज्य का पैसा खर्च हो जाता है।
राज्य को खर्च करने के लिए सख्त राजकोषीय सीमाओं (Fiscal Limits) का पालन करना होता है। 2025-26 के लिए, कुल अनुमानित खर्च ₹2.94 लाख करोड़ है, जबकि अनुमानित कमाई (Revenues) सिर्फ ₹2.61 लाख करोड़ है। खर्च और कमाई का यह अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है, जिसे GSDP के 2.98% पर नियंत्रित रखना होता है। ये सीमाएँ साफ़ बताती हैं कि राज्य के पास खर्च करने की गुंजाइश न के बराबर है।
वर्तमान प्रतिबद्ध खर्च और विकास की कुर्बानी
बिहार के बजट का बड़ा हिस्सा पहले से ही ‘प्रतिबद्ध खर्च’ (Committed Expenditure) में फँसा हुआ है। 2023-24 में, राज्य की कुल कमाई का 36% हिस्सा इन अनिवार्य खर्चों में लगा:
वेतन (Salary): 20% ,पेंशन: 13%, ब्याज भुगतान: 9%
2025-26 में भी, वेतन पर करीब ₹51,690 करोड़ और पेंशन पर ₹33,389 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
इतना सारा पैसा राजस्व खर्च (वेतन, पेंशन) में जाने का सबसे बुरा असर पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर पड़ता है। पूंजीगत व्यय वह खर्च है जिससे नए स्कूल, कॉलेज, सड़कें और अस्पताल बनते हैं—यानी यही राज्य के विकास का असली इंजन है। 2023-24 में, कुल खर्च में पूंजीगत व्यय का हिस्सा सिर्फ 20.63% था। अगर वेतन भुगतान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, तो यह 20% का हिस्सा और भी सिकुड़ जाएगा, जिससे विकास का पहिया पूरी तरह थम जाएगा।
वित्तीय दिवालियापन
कोई भी राज्य, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी, बिना किसी विशाल नए आय स्रोत के इतना खर्च नहीं उठा सकती। यह स्थिति राज्य के लिए गारंटीशुदा दिवालियापन (Bankruptcy) है। अगर सरकार यह वादा पूरा करने की कोशिश करती है, तो उसके सामने दो ही विनाशकारी विकल्प होंगे:
बुनियादी ढांचे का खात्मा
राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सड़क, और सिंचाई जैसी सभी ज़रूरी सेवाओं के लिए पूंजीगत खर्च और मौजूदा गैर-विकास खर्च को पूरी तरह से शून्य करना होगा। इससे राज्य में सभी विकास और कल्याणकारी गतिविधियाँ ठप्प हो जाएँगी।
अत्यधिक कर्ज और डिफॉल्ट: राज्य को हर साल ₹25 लाख करोड़ से ज़्यादा का भारी कर्ज लेना होगा। यह कदम राज्य के कर्ज को GSDP के अनुपात में 37.04% से बढ़ाकर 300% या उससे ज़्यादा कर देगा। इस पैमाने पर कर्ज लेने का मतलब है कि केंद्र सरकार से वित्तीय मदद तुरंत रुक जाएगी, और बिहार प्रभावी रूप से वित्तीय रूप से दिवालिया हो जाएगा।
असंभव समय सीमा
करोड़ों लोगों की भर्ती 20 महीने की समय सीमा में करना प्रशासनिक रूप से भी असंभव है। इसका मतलब है कि हर महीने 12.5 लाख लोगों को सफलतापूर्वक चुनना, दस्तावेज़ों की जाँच करना और नौकरी पर रखना। सरकारी प्रक्रियाएँ, जो पारदर्शिता और कानूनी चुनौतियों के कारण वैसे भी धीमी होती हैं, इस गति को कभी हासिल नहीं कर सकतीं।
इतनी कम अवधि में बड़े पैमाने पर भर्ती करने का प्रयास गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता करवाएगा:
परीक्षा में गिरावट: निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करना और उनके परिणाम समय पर जारी करना असंभव होगा। इससे यह तय है कि योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाएगा, और चयन का आधार योग्यता (Merit) के बजाय अनुचित कारक बन जाएँगे।
व्यापक भ्रष्टाचार: जब नौकरी की माँग (Demand) संसाधन की आपूर्ति (Supply) से कई गुना ज़्यादा होती है, तो चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धांधली की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
अयोग्य प्रशासन: यदि गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, तो राज्य के प्रशासन में बड़े पैमाने पर अयोग्य कर्मचारी भर जाएँगे। इसका सबसे बुरा असर सरकारी सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और कानून व्यवस्था की गुणवत्ता पर पड़ेगा, जिससे राज्य की प्रगति दशकों पीछे चली जाएगी।
यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं: ‘फ्रीबीज़’ का राष्ट्रीय चलन
चुनावी वादे, जिन्हें ‘फ्रीबीज़’ (मुफ्त चीज़ें) कहा जाता है, अब केवल RJD या बिहार तक सीमित नहीं हैं। यह एक राष्ट्रीय चलन बन गया है, जहाँ राजनीतिक लाभ के लिए देश के राजकोषीय स्वास्थ्य को दाँव पर लगाया जाता है।
अन्य लोकलुभावन वादे: अन्य दलों ने भी ऐसे वादे किए हैं, जैसे मुफ्त बिजली देना, बेरोजगारों को मासिक वजीफा देना या महिलाओं को नकद हस्तांतरण (जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना)।
मध्य प्रदेश का उदाहरण: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का बजट भी ₹10,800 करोड़ था। इस योजना ने चुनावी सफलता ज़रूर दी, लेकिन राज्य पर राजकोषीय दबाव बढ़ाया है, और राज्य का कर्ज ₹4 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
पैमाने का अंतर: लाडली बहना योजना या मुफ्त बिजली जैसी योजनाएँ राजकोषीय रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन वे अभी भी राज्य के बजट के एक छोटे हिस्से में आती हैं। इसके विपरीत, RJD का ₹27.75 लाख करोड़ का अनुमानित वादा वित्तीय जोखिम की सीमा से परे, ‘पूर्ण कल्पना’ की श्रेणी में आता है।
अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुफ्त पैसा डालने से महँगाई (Inflation) बढ़ती है, और यह अंततः सभी नागरिकों पर बोझ डालती है। ‘फ्री’ कुछ भी नहीं होता; इसका भुगतान या तो ज़्यादा टैक्स से होता है या फिर खराब सड़कों और स्कूलों से (क्योंकि विकास बजट में कटौती होती है)।